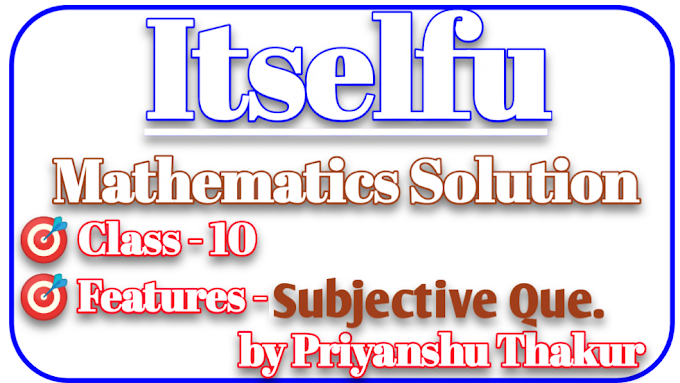एनसीईआरटी कक्षा 10 विज्ञान अध्याय 15 - हमारे पर्यावरण संशोधन नोट्स
- पर्यावरण का अर्थ है वह सब कुछ जो हमें घेरता है। इसमें सजीव (जैविक) और निर्जीव (अजैविक) घटक शामिल हो सकते हैं।
- जैविक: पौधे और जानवर। अजैविक : वायु, जल आदि।
- पर्यावरण किसी जीव के प्राकृतिक आवास में उसके जीवन और विकास को प्रभावित करता है और इसके विपरीत।
- वे पदार्थ जो जीवाणु जैसे सूक्ष्म जीवों की क्रिया से अपघटित हो सकते हैं, जैव अपघटनीय कहलाते हैं। जैसे जैविक कचरा।
- वे पदार्थ जो सूक्ष्मजीवों की क्रिया से विघटित नहीं हो सकते, अजैव निम्नीकरणीय कहलाते हैं।
- जैव निम्नीकरणीय कचरे के उदाहरण: गोबर, कपास, जूट, कागज, फलों और सब्जियों के छिलके, पत्ते आदि।
- गैर-बायोडिग्रेडेबल कचरे के उदाहरण: प्लास्टिक, पॉलिथीन बैग, सिंथेटिक फाइबर, धातु, रेडियोधर्मी कचरा।
ईको सिस्टम और इसके घटक
- किसी क्षेत्र में परस्पर क्रिया करने वाले सभी जीव निर्जीव घटकों के साथ मिलकर एक पारितंत्र का निर्माण करते हैं। तो एक पारिस्थितिकी तंत्र में जैविक (जीवित प्राणी) और अजैविक घटक जैसे तापमान, वर्षा, हवा, मिट्टी आदि दोनों होते हैं।

- सभी जीवित जीवों को पोषण के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है।
- I. उत्पादक: सभी हरे पौधे, नीले हरे शैवाल प्रकाश ऊर्जा (प्रकाश संश्लेषण) का उपयोग करके अकार्बनिक पदार्थ से अपना भोजन (चीनी और स्टार्च) उत्पन्न कर सकते हैं।
द्वितीय. उपभोक्ता : ऐसे जीवों को शामिल करें जो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से अपनी जीविका के लिए उत्पादकों पर निर्भर हैं। उपभोक्ता भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर हैं।
III. अपघटक : कवक और जीवाणु जो मृत पौधे को तोड़ते हैं (अपघटित होते हैं),
जंतु जटिल यौगिकों को सरल में बदल देते हैं। इस प्रकार डीकंपोजर पुनःपूर्ति में मदद करते हैं
ए 3-चरणीय खाद्य श्रृंखला - खाद्य श्रृंखला : यह जीवित जीवों का वह क्रम है जिसमें एक जीव ऊर्जा के लिए दूसरे जीव का उपभोग करता है। यह यूनिडायरेक्शनल (एकल दिशात्मक) है।

- एक खाद्य श्रृंखला में, विभिन्न चरणों में जहां ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, पोषी स्तर कहलाता है।
- हरे पौधे सूर्य की 1% ऊर्जा पर कब्जा कर लेते हैं।
- खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह एकदिशीय होता है।
- एक खाद्य श्रृंखला में एक पोषी स्तर से अगले पोषी स्तर तक ऊर्जा की मात्रा में क्रमिक कमी होती है।

- 10 प्रतिशत नियम: प्रत्येक क्रमिक पोषी स्तर पर उपलब्ध ऊर्जा पिछले स्तर का 10% है।
- खाद्य श्रृंखला में प्रत्येक अगले पोषी स्तर के साथ हानिकारक रसायनों की सांद्रता बढ़ जाती है। इसे कहते हैं जैव आवर्धन
- ऐसे रसायनों की अधिकतम सांद्रता मानव शरीर में जमा हो जाती है। चूँकि मनुष्य किसी भी खाद्य श्रृंखला में शीर्ष स्तर पर होता है।
- पर्यावरण में परिवर्तन हमें प्रभावित करते हैं और हमारी गतिविधियाँ हमारे आसपास के वातावरण को बदल देती हैं। मनुष्यों के कारण होने वाली पर्यावरणीय समस्याएं:
- (O3) परत काफी हद तक समताप मंडल में पाई जाती है जो समुद्र तल से 12 किमी - 50 किमी ऊपर हमारे वायुमंडल का एक हिस्सा है।
- जमीनी स्तर पर ओजोन एक घातक जहर है।
- ओजोन निम्न प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया के परिणामस्वरूप बनता है।
- ओजोन परत पृथ्वी के चारों ओर एक सुरक्षात्मक आवरण है जो सूर्य के अधिकांश हानिकारक यूवी (पराबैंगनी) विकिरण को अवशोषित करती है, इस प्रकार पृथ्वी के जीवित प्राणियों को त्वचा के कैंसर, आंखों में मोतियाबिंद, कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली, पौधों के विनाश आदि जैसे स्वास्थ्य खतरों से बचाती है। .
- अंटार्टिका में ओजोन परत की मोटाई में गिरावट पहली बार 1985 में देखी गई थी और इसे ओजोन छिद्र कहा गया था।
- खुले में डंपिंग: एक पारंपरिक तरीका जिसमें ठोस कचरे को शहर के चुनिंदा क्षेत्रों में डंप किया जाता है। यह वास्तव में प्रदूषण का कारण बनता है
- भूमि भराव : कचरे को कम रहने वाले क्षेत्र में डंप किया जाता है और बुलडोजर के साथ घुमाकर जमा किया जाता है
- कम्पोस्टिंग : जैविक कचरे को एक कम्पोस्ट पिट (2m × 1m × 1m) में भरा जाता है। फिर इसे मिट्टी की एक पतली परत से ढक दिया जाता है। करीब तीन महीने बाद गड्ढे के अंदर भरा वही कचरा जैविक खाद में बदल जाता है।
- पुनर्चक्रण (Recycling ) : ठोस अपशिष्ट अपने संघटक सरल पदार्थों में टूट जाता है। इन सामग्रियों का उपयोग फिर नई वस्तुओं को बनाने के लिए किया जाता है। यहां तक कि प्लास्टिक, धातु जैसे गैर-जैव अपघटनीय ठोस अपशिष्टों को भी पुनर्चक्रित किया जा सकता है।
- पुन : उपयोग: किसी वस्तु को बार-बार उपयोग करने की एक बहुत ही सरल पारंपरिक तकनीक। उदाहरण के लिए लिफाफा आदि बनाने के लिए कागज का पुन: उपयोग किया जा सकता है।
अतः केवल 10% ऊर्जा ही अगले पोषी स्तर पर स्थानांतरित होती है जबकि 90% ऊर्जा वर्तमान पोषी स्तर द्वारा अपनी जीवन प्रक्रियाओं में उपयोग की जाती है।
पर्यावरणीय समस्याएँ
(ए) ओजोन परत की कमी और अपशिष्ट निपटान।
(बी) अपशिष्ट निपटान के कुप्रबंधन के कारण प्रदूषण।
I. ओजोन परत का अवक्षय
ओजोन क्षरण का कारण
सीएफसी (क्लोरो फ्लोरो कार्बन) एक सिंथेटिक, अक्रिय रसायन जैसे फ्रीऑन का अत्यधिक उपयोग, जो रेफ्रिजरेंट के रूप में और आग बुझाने के यंत्रों में उपयोग किया जाता है, ऊपरी वातावरण में ओजोन की कमी का कारण बना। एक एकल क्लोरीन परमाणु 1,00,000 ओजोन अणुओं को नष्ट कर सकता है। UNEP (संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम) ने सभी देशों द्वारा 1986 के स्तर (KYOTO प्रोटोकॉल) पर CFC उत्पादन को स्थिर करने के लिए एक समझौता करने में एक उत्कृष्ट कार्य किया।
कचरा निपटान
औद्योगीकरण और उपभोक्ता वस्तुओं की मांग में वृद्धि ने विशेष रूप से शहरी क्षेत्र में अपशिष्ट/कचरा संचय और इसके निपटान के रूप में एक बड़ी समस्या पैदा कर दी है।
दुनिया भर में आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाले ठोस अपशिष्ट निपटान के विभिन्न तरीके
हैं।